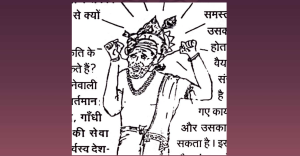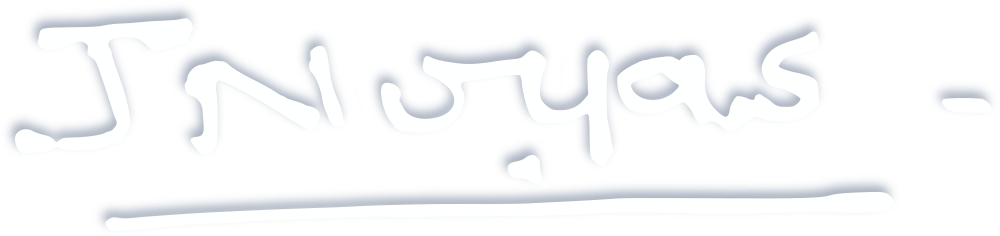श्री रामकृष्ण परमहंस एक बार भाव-समाधि की स्थिति में थे । उनके मुख से ‘शिव-ज्ञाने जीव-सेवा’ ये उद्गार प्रवाहित हुए । उन्होंने कहा, ‘दया नहीं, दया नहीं, जो शिव सभी प्राणियों में निवास करता है उसके ज्ञान से सम्पन्न होकर, प्राणिमात्र की सेवा करो – सेवा करना ही उचित है’ ।
स्वामी विवेकानन्द इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग इस कथन के महत्व को समझाने में और उसको क्रियान्वित करने में लगा दिया । स्वामी शिवानन्द ने कहा कि रामकृष्ण मिशन द्वारा किये गए अगणित सेवा कार्य का स्रोत क्या है, ऐसा प्रश्न यदि कोई पूछे तो उसको इसका उत्तर परमहंस के उद्गारों में मिल जाएगा । कहने की आवश्यकता नहीं कि आज उनके नाम पर चलने वाली अनेक ऐसी संस्थाएँ हैं जो सेवा का कार्य निःस्वार्थ भाव से देश के कोने-कोने में कर रही हैं ।
परमहंस के इन उद्गारों में दो महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं । भूत-दया का भाव अत्यन्त उदात्त है, परन्तु उसमें यह दोष है कि दया करनेवाले के मन में ‘मैं दया करता हूँ’ ऐसा अहंकार उत्पन्न हो सकता है । इसके विपरीत सेवा के भाव में अहंकार के स्थान पर विनम्रता आती है । इसके अतिरिक्त सेवा-कार्य में लगा व्यक्ति यह जानता है कि वह यह सेवा स्वयं अपने हित-साधन की दृष्टि से करता है, किसी पर उपकार नहीं करता । सेवा का अवसर देनेवाले प्राणियों के प्रति उसका यह विनीत भाव उसे निरहंकारी, निःस्वार्थ और विनम्र बनाता है ।
इसके अतिरिक्त एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की सेवा ‘नर में जो नारायण’ स्थित हैं उनके प्रति समर्पित होती है । इसी कारण उसमें प्रेम, आदर और भक्ति-भाव का समावेश हो जाता है । वे उस अन्तर्यामी नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और इसलिए उनकी मानव-सेवा प्रकारान्तर से देव-सेवा ही होती है ।
सेवा का यह उदात्त रूप प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है । सामान्य लोगों के लिए ‘नर में स्थित नारायण’ का प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होना सम्भव नहीं है । इसलिए हम जैसे सामान्य लोगों का सेवा-कार्य अलौकिक, आध्यात्मिक धरातल पर स्थित न होकर नैतिक धरातल पर ही सम्भव हो सकता है । हम यह मानकर कि प्रत्येक व्यक्ति में देवी अंश विद्यमान है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति हमारी सेवा प्राप्त करने का अधिकारी है, सेवा-कार्य इसी भावना से कर सकते हैं । हमारे कर्म हमारे मन में तदनुरूप भावों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखते हैं । यह सर्वविदित है कि हमारे भावों या संवेगों का आवेग हमें कर्म-प्रवृत्त करता है । परन्तु कई बार हमारे कर्म भी तदनुरूप भावों की उत्पत्ति के कारण बन जाते हैं और इसीलिए इस भावना से किये गए सेवा-कर्म भी फलदायी सिद्ध होते हैं ।
सेवा के जिन रूपों का आध्यात्मिक स्तर पर (या) नैतिक धरातल पर हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनकी दो विशेषताएँ हैं:
सेवा करनेवाले व्यक्ति को यह आभास रहता है कि वह यह सेवा स्वयं अपने हित-साधन की दृष्टि से कर रहा है और इसीलिए वह इस सेवा द्वारा किसी पर कोई उपकार नहीं करता ।
सेवा में प्रधान रूप में (आध्यात्मिक) प्रेम और आदर का भाव रहता है और गौण रूप में (नैतिक) कर्त्तव्य की भावना का बल रहता है ।
दोनों ही रूपों में सेवा निस्वार्थ होती है, अतएव उसमें प्रतिफल प्राप्त करने की कोई आकांक्षा या आशा को स्थान नहीं रहता । सेवा के ये दोनों रूप शुद्ध भारतीयता के प्रतीक या उदाहरण कहे जा सकते हैं ।
पाश्चात्य सभ्यता के आने के पश्चात् सेवा का अर्थ ही विकृत हो गया । सेवा को सर्विस (𝓈ℯ𝓇𝓋𝒾𝒸ℯ) का पर्याय मानकर उसे उसके संकुचित अर्थ में प्रयोग करने का प्रचलन ज़ोर पकड़ने लगा । ‘सेवा’ का यह अर्थ-परिवर्तन दो रूपों में परिलक्षित होता है ।
पहला रूप तो वह है जिसमें वेतनभागी कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य आता है अथवा मूल्य प्राप्त करके की गई किसी की सहायता । डॉक्टर द्वारा की गई चिकित्सा, शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा, मूल्य लेकर खरीदी या बेची जानेवाली वस्तु, विनिमय का कार्य आदि । आज दुकानों में, होटलों में, सरकारी कार्यालयों में इसी प्रकार की सेवा प्रचलित है । ‘हमारे योग्य सेवा’ ‘हमें भी सेवा करने का एक अवसर दीजिए’ या इनसे मिलते-जुलते अर्थ के वाक्य पढ़ने को मिल जायेंगे । यह सेवा सशुल्क होती है और उसे कोई भी क्रय कर सकता है यदि उसमें उसका पूरा मूल्य चुकाने की सामर्थ्य हो । वास्तव में यह सेवा, सेवा न होकर या तो नौकरी-चाकरी है या व्यापार-धन्धा ।
यह सेवा या सेवा का यह प्रकार पाश्चात्य सभ्यता की देन है । इस प्रकार की सेवा आज कैसे की जाती है, इसे किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं । हम सभी इसके भुक्तभोगी हैं । नौकरी अथवा व्यापार के अर्थ में भी यह इतनी विकृत हो गई है कि इसे सेवा कहने में ही हिचकिचाहट होती है । इसमें धोखाधड़ी और छल-कपट इतनी मात्रा में है कि उसे भारतीय मनीषी व्यापार-धन्धा या नौकरी-चाकरी भी कहने में संकोच का अनुभव करेंगे ।
दूसरा परिवर्तन जो सेवा के अर्थ में आया है वह भी कुछ कम चमत्कारिक नहीं है । जाति की सेवा, समाज की सेवा, देश व राष्ट्र की सेवा और न जाने कितने नवीन से नवीनतम सेवा-क्षेत्रों का आविष्कार प्रतिदिन किया जाता है । यह सेवा राजकीय सहायता प्राप्त करके, समाज या व्यक्तियों से वसूल करके या अन्य प्रकार से धन-संग्रह करके की जाने लगी है और इस प्रकार सेवा ने धन्धे का रूप धारण कर लिया है । जो अन्य किसी भी कार्य करने की क्षमता नहीं रखते वे समाज-सेवा या देश-सेवा का धन्धा शुरु कर अपने लिए अर्थोपार्जन का साधन जुटा लेते हैं । परिणाम यह होता है कि समाज में धोखाधड़ी, छीना-झपटी और शोषण जैसे घृणित कार्य भी समाज-सेवा के नाम पर खुलकर किये जाते हैं । आज भारत में ऐसे समाज-सेवियों की बाढ़ सी आ गई है और नगर-नगर या ग्राम-ग्राम में ऐसे समाज-सेवी या ऐसी समाज-सेवी संस्थाएँ पनपती जा रही हैं । आज उनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं है । जिसकी सेवा की जा रही है वह अधिकाधिक असहाय, विपन्न और दुःखी होता जा रहा है एवं जो सेवा करनेवाले हैं वे अकूत सम्पत्ति के स्वामी बनते जा रहे हैं । देश-सेवा भी उच्च पद और उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं के अभाव में सम्भव ही नहीं लगती । यहाँ तक कि आकस्मिक प्राकृतिक विपदाओं में सहायतार्थ प्राप्त सम्पत्ति को भी सुरक्षित समझना आज साहस का कार्य हो गया है । आज सबको धन चाहिए, चाहे वह किसी भी रीति से क्यों न प्राप्त हुआ हो ।
सेवा के ये दोनों रूप भारतीय संस्कृति के अनुरूप सेवा से किस प्रकार मेल खा सकते हैं?
यदि हम पौराणिक कहानियाँ या सही लगनेवाली प्राचीन घटनाओं को छोड़ भी दें तो भी वर्तमान युग में भी परमहंस और विवेकानन्द, गाँधी और विनोबा जैसे समाज व देश की सेवा करनेवाले हो गए हैं । जिन्होंने अपना सर्वस्व देश-सेवा, समाज-सेवा अथवा अपने आदर्श की भेंट चढ़ा दिया था, जिन्होंने अपमान और तिरस्कार सहन करके भी सेवा कार्य किया था । सौभाग्य की बात यह है कि आज भी देश में ऐसे व्यक्तियों की या समाज-सेवी संस्थाओं का सर्वथा अभाव नहीं है जो निःस्वार्थ भाव से जन-जन के कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं । इस आदर्श को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है । वैयक्तिक स्तर पर हम उनको सहयोग देकर, उनके कार्यों में रुचि लेकर व यथासम्भव सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करके उनको अधिक कुशलता से सेवा-कार्य करने का अवसर दे सकते हैं ।
हमने ऊपर सेवा के भारतीय आदर्श के दो रूपों का उल्लेख किया है । प्रथम रूप सभी सामान्य लोगों की पहुँच के बाहर होने से कुछ बिरले महानुभाव ही उसका प्रयोग कर सकते हैं । उनको न नियमों की आवश्यकता है न निर्देशों की । उनके हृदय में स्थित देव ही उनकी समस्त क्रियाओं का संचालन करता है । अतः उसका कार्य सदैव लोकोपकारी व त्रुटिरहित होता है ।
परन्तु दूसरे प्रकार का सेवा कार्य वैयक्तिक स्तर पर भी हो सकता है और संस्थागत संगठित रूप में भी हो सकता है । निःसन्देह संस्था के माध्यम से किये गए कार्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो सकता है और उसका लाभ भी अधिक लोगों को प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार के सेवा कार्य में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उस कार्य को ईश्वर के प्रति सेवा या समाज के प्रति अपना कर्त्तव्य समझकर निस्वार्थ भाव से, शालीनता और विनम्रता से सम्पादित करें । इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में उसको अर्थोपार्जन का साधन समझने की भूल न करें । हमें समाज का यह ऋण चुकाना है, इस भाव से ईश्वरार्पण अथवा देवाराधना समझकर किया गया सेवा-कार्य ही सच्चा सेवा-कार्य हो सकता है ।
जगन्नाथ व्यास भजन चौकी, जोधपुर।